एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के मानसिक एवं दैहिक जीवन का अध्ययन करता है। व्यवहार में मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है इसलिये इस को आत्मा का विज्ञान भी कहा जाता है।
शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है-शिक्षा व मनोविज्ञान । शिक्षा – ‘शिक्षा’ शब्द का अंग्रेजी अनुवाद ‘Education’ है जिसकी ‘उत्पत्ति ‘Educatum’ से मानी जाती है, जिसमें मूल शब्द ‘E’ तथा ‘duco’ है। ‘E’ का अर्थ है अंदर से तथा ‘duco’ का अर्थ है बाहर निकालना। अर्थात् शिक्षा का अर्थ है बालक की अंतर्निहित क्षमताओं का प्रदर्शन करवाने की प्रक्रिया।
- Advertisement -
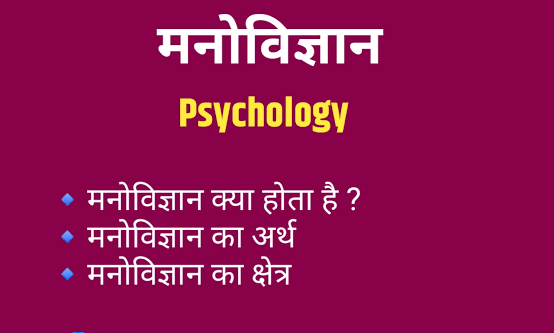
मनोविज्ञान का अर्थ
मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शनशास्त्र (Philosophy) से मानी जाती है लम्बे समय तक इसका दर्शनशास्त्र के रूप में ही अध्ययन होता रहा बाद में इसे एक स्वतंत्र ‘ विषय ‘ के रूप में माना गया । एविंगहास (Ebhinghaus ) ने कहा — ” मनोविज्ञान का भूतकाल अत्यंत लम्बा है परन्तु इसका इतिहास बहुत ही छोटा है “। मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया परन्तु समय के साथ में परिवर्तन होते रहे है जो कि निम्नलिखित चार अवस्थाओ के रूप में समझे जा सकते है —
मनोविज्ञान क्या है अर्थ 10 परिभाषाएँ 5 Easy Methods in Psychology (What Is Psychology in Hindi)
- आत्मा के अध्ययन के रूप में – ग्रीक के दार्शनिक डेमोक्रोटस,प्लेटो,अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में दर्शनशास्त्र के जैसा बताया है परन्तु आप भी जानते है कि आत्मा सूक्ष्म में ,इसे न देखा जा सकता है,ना ही छुआ जा सकता है , ना ही इस पर कोई वैज्ञानिक प्रयोग किये जा सकते है । चूँकि इन दार्शनिको द्वारा आत्मा के सम्बंध में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नही किया जा सका इसलिए इसे मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में स्वीकार नही किया गया तथा इसके अर्थ में परिवर्तन की दूसरी अवस्था का विकास हुआ ।
- मन के अध्ययन के रूप में – जर्मन दार्शनिक ‘कांत’ ने मनोविज्ञान को मन के अध्यअध्ययन के रूप में परिभाषित किया है परन्तु मन शब्द में एक स्पष्ट अर्थ प्रकट नही करता इसलिये इसको भी पूरी तरह से स्वीकार नही किया गया । पैम्पॉनाजी, लॉक, लिबिनिज भी इस मत के समर्थन में थे इनके मत के अस्वीकार होने के बाद की अगली अवस्था का विकास हुआ ।
- चेतना के विज्ञान के रूप में – विल्हेम वुंट तथा विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को “चेतना के विज्ञान” के रूप में परिभाषित किया है इसी अवस्था में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में जाना जाता है । विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक ‘ मनोविज्ञान के सिद्धांत ‘ एक ऐसे विषय के रूप में प्रस्तुत किया है जिसमे चेतना की अवस्थाओ का विवरण प्रस्तुत किया है । उन्होंने ने चेतना की धारा का संप्रत्यय भी प्रस्तुत किया है जो कि काफी प्रचलित है । विलयम वुंट ने भी ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है जिसमे ‘ आंतरिक अनुभवों ‘ का अध्ययन किया जाता है । परन्तु इन सबके विपरीत सिगमंड फ्रायड ने यह प्रतिपादित किया कि चेतना के तीन स्तर होते है – 1.चेतन, 2.अवचेतन, 3. अचेतन फ्रायड के अनुसार सिर्फ चेतन का अध्ययन करना व्यवहार के अध्ययन के लिये लाभदायक नही है । इन्होंने चेतना को अस्वीकार करते हुये अचेतन की भूमिका पर बल दिया है इसलिये आखिर में इस अर्थ में भी परिवर्तन किया गया
- व्यवहार के विज्ञान के रूप में – 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब जब मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, तब उसे व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया । व्यवहार शब्द को जे.बी. वाटसन द्वारा प्रचलित किया गया ।इस अर्थ के अन्य मुख्य समर्थक मैकडुगल तथा पिल्सबरी थे ।https://hihindi.com/what-is-psychology-in-hindi/
मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ
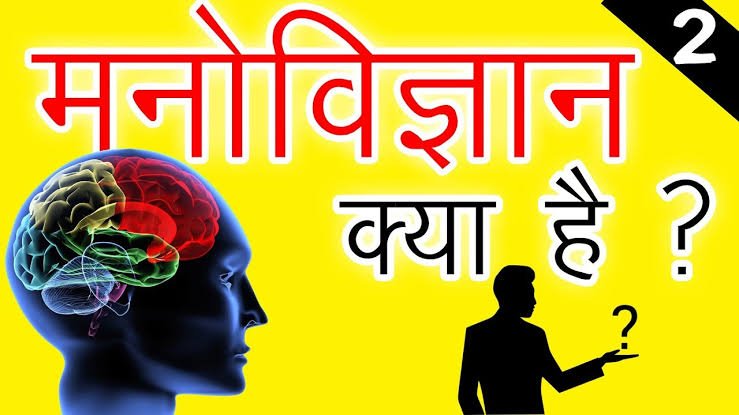
मन+विज्ञान = मनोविज्ञान यह वह विज्ञान है जिसमे प्राणियों के मन ओर विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है अंग्रेजी भाषा मे मनोविज्ञान के लिये Psychology शब्द का प्रयोग किया जाता है
- Psyche साइके = आत्मा
- Logos लोगोस = अध्ययन
- मतलब आत्मा (मन) का अध्ययन
आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि इसकी उत्पत्ति दर्शनशास्त्र से हुई है इसके बाद अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स ने 1842-1910 ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से मुक्त कर एक स्वतंत्र विद्या का रूप दिया ।
- Advertisement -
मनोविज्ञान की परिभाषाएं (Psychology Definitions)
अलग – अलग शोधकर्ताओं ने अपने मत के अनुसार अलग – अलग मत प्रकट किये है जो कि निम्नलिखित है ।
- स्किनर (Skinner) — “ व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है ।”
- वाटसन (Watson) — “ व्यवहार का निश्चित विज्ञान है।”
- क्रो एवं क्रो (Crow and Crow) — ” मानव व्यवहार और मानव सम्बन्धो का अध्ययन करता है”।
- मैकडूगल (McDougall) — “मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है”।
- मन (Munn) — ” आधुनिक मनोविज्ञान का सम्बंध, व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से”।
- जेम्स (James) — “मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन ओर व्यख्यान के रूप में की जा सकती है” ।
- गैरिसन व अन्य (Garrison and others) — “मनोविज्ञान का सम्बंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है”।
- पिल्सबरी (Pillsburry) — ” सबसे संतोषजनक परिभाषा,मानव व्यवहार में विज्ञान के रूप में की जा सकती है”।
- वुडवर्थ (Woodworth ) — “मनोविज्ञान, वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है”।
मनोबिज्ञान का शिक्षा में उद्देश्य –
परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किये जाते हैं। मानवीय प्रकृति की जीवन की अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग आवश्यकताएँ होती हैं। इनके आधार पर शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य माने जाते हैं
1.ज्ञान प्रदान करने का उद्देश्य (Aim of providing knowledge) बौद्धिक विकास के लिए ज्ञान आवश्यक है। इसके अलावा जीवन में बेहतर समायोजन के लिए, सामाजिक निपुणता के लिए, चरित्र निर्माण के लिए तथा आध्यात्मिक चेतना के लिए भी ज्ञान आवश्यक है। अतः शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को ज्ञान उपलब्ध कराना होता है।
2.व्यवसाय चुनने का उद्देश्य (Aim of choosing occupation) – सभी व्यक्तियों को अपना संरक्षण करने की आवश्यकता होती है अतः शिक्षा द्वारा व्यक्ति को उसकी रोजी-रोटी प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा किया जाता है।
3.व्यक्तित्व के संतुलित विकास का उद्देश्य – पैस्टालॉजी (Pestalozzi) ने शिक्षा को मस्तिष्क, हृदय तथा हाथों के संतुलित विकास के रूप में परिभाषित किया है। इसी प्रकार गाँधी (Gandhi) ने भी व्यक्ति के शरीर, मन तथा आत्मा को विकसित करने पर बल दिया है।
4.पूर्ण जीवन का उद्देश्य (Aim of fullfilled life) यह उद्देश्य हरबर्ट स्पेन्सर (Herbert Spencer) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उनके अनुसार पूर्ण जीवन के अन्तर्गत पाँच क्रियाएँ सम्मिलित हैं आत्म संरक्षण, व्यवसाय का चुनाव, अपने घर के महत्वपूर्ण सदस्य होना, समाज में अपना योगदान देना तथा खाली समय को बेहतर रूप में प्रयोग करना ।
5.चरित्र निर्माण का उद्देश्य (Aim of character formation) – जॉन ड्यूवी (John Dewey) ने चरित्र निर्माण को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार शिक्षा द्वारा मनुष्य को एक असामाजिक तथा असंस्कृत व्यक्तित्व से एक मानवीय तथा सामाजिक स्तर पर पहुँचाना होता है।
6.व्यक्तिगत उद्देश्य (Personal Aim) नन (Nunn), रूसो (Rousseau) तथा हरबर्ट (Herbert) ने शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य 3को महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार शिक्षा द्वारा व्यक्ति की जन्मजात
शक्तियों तथा सम्भावनाओं का पूर्ण विकास होना आवश्यक है।
मनोविज्ञान के सम्प्रदायक
| नाम | संस्थापक | उत्पत्ति का स्थान |
| संरचनावाद | टिचनर/वुंट | जर्मनी |
| प्रकार्यवाद | विलियमजेम्स | अमेरिका |
| गेस्टालवाद | मैक्स वर्दीमर | जर्मनी |
| व्यवहारवाद | जे०बी० वाटसन | अमेरिका |
| मनोविश्लेषणात्मक | सिंगमण्ड फ्रायड | आस्ट्रिया |
| मानवतावादी | अब्राहम मैस्लो | अमेरिका |
मनोविज्ञान की विधियाँ
मानव व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। अध्ययन या शोध का मुख्य उद्देश्य नियमों तथा सिद्धान्तों को विकसित करना, उनका परीक्षण करना तथा विभिन्न मानवीय समस्याओं के समाधान हेतु उन्हें अनुप्रयुक्त करना होता है।
वैज्ञानिक रूप से जो शोध मनोविज्ञान में किये जाते हैं उनकी निम्नलिखित मुख्य विशेषताएँ होती हैं
वस्तुनिष्ठता (Objectivity) — जिसका अर्थ है कि इस प्रकार के शोध किसी भी प्रकार के पक्षपात से स्वतंत्र होते हैं।
परीक्षण योग्य (Testable) – ऐसे शोध किसी के भी द्वारा परीक्षण के लिए उपलब्ध होते हैं। उन शोधों की प्रमाणिकता को सिद्ध करने हेतु कोई भी अन्य व्यक्ति वही विधि अपनाकर शोध को दोहराकर जाँच कर सकता है।
आत्म-संशोधन (Self Correction) – ऐसे सिद्धांतों में यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो शोधकर्ता उस त्रुटि को सुधारने की पूर्ण कोशिश करता है।
मनोविज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन किये जाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। उनमें से कुछ मुख्य विधियाँ निम्नलिखित हैं
1.निरीक्षण विधि/ बाह्यदर्शन विधि (Observation/Extrospection Method) – निरीक्षण वह विधि है जिसमें घटनाओं को क्रमबद्ध पंजीकृत किया जाता है तथा इस दौरान जिस घटना का अध्ययन किया जाता है उससे संबंधित चरों (Variables) की कार्यप्रणाली में जानबूझकर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। अतः घटना से संबंधित चरों को जैसे वे हैं उसी रूप में अंकित किया जाता है। निरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान, निम्नलिखित चरणों को सामान्यतः सम्मिलित किया जाता है (a) निरीक्षण किये जाने वाले व्यवहार का चुनाव तथा नियोजन । (b) चुने/चयनित किये गए व्यवहार का निरीक्षण व रिकॉर्ड करना । (c) निरीक्षण किये गए व्यवहार का विश्लेषण व व्याख्या करना । (d) सामान्यीकरण।
2.प्रयोग विधि (Experiment Method) प्रयोग विधि व्यवहार के अध्ययन हेतु सर्वाधिक वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ विधि मानी जाती है। एक प्रयोग में, प्रयोगकर्ता एक चर (Variable) में जानबूझ कर या यकायक किये गए जोड़तोड़ (Deliberate Manipulation) के दूसरे चर पर पड़ रहे प्रभाव का अध्ययन करता है। अतः, प्रयोग वह विधि है जिसके द्वारा चरों के बीच ‘कारण तथा प्रभाव सम्बन्ध (Cause and effect relationship) की व्याख्या की जा सकती है।’
3. केस-अध्ययन विधि (Case Study Method) इस विधि में विश्लेषण की मुख्य इकाई व्यक्ति तथा जीवन के संदर्भ में उसके विभिन्न अनुभव होते हैं। इस विधि में व्यक्ति तथा उससे संबंधित महत्त्वपूर्ण लोगों के साथ अंतर्क्रियात्मक तरीकों तथा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उसके व्यक्तिगत अनुभवों पर बल दिया जाता है।
किसी व्यक्ति का जीवन-वृत (Case History) तैयार करने के लिए विभिन्न स्रोतों से आँकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। उदाहरण के लिए उसका पारिवारिक इतिहास (Family History), शैक्षिक जीवन (Educational Life), चिकित्सीय इतिहास (Medical History) तथा सामाजिक जीवन (Social Life) आदि। यह विधि नैदानिक मनोविज्ञान (Clinical Psychology) तथा जीवन-अवधि विकासात्मक मनोविज्ञान (Life span Developmental Psychology) में काफी प्रसिद्ध है।
4.साक्षात्कार विधि (Interview Method)साक्षात्कार शब्द का प्रयोग सामान्यतः काफी किया जाता है। यह आँकड़ों के संग्रहण की वह तकनीक है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच कुछ निर्धारित उद्देश्यों के साथ आमने-सामने की अंतर्क्रिया होती है। जो व्यक्ति साक्षात्कार का क्रियान्वन करता है उसे साक्षात्कारकर्ता (Interviewer) कहा जाता है जबकि जिस व्यक्ति को साक्षात्कारकर्ता के प्रश्नों के प्रति अनुक्रिया देनी होती है उसे इंटरव्यूई / प्रयोज्य (Interviewee) कहा जाता है।
आमने-सामने की स्थिति के अलावा, साक्षात्कारों का क्रियान्वयन टेलीफोन, इन्टरनेट तथा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से भी किया जाता है। साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे अभिवृत्तियों, मूल्यों, रुचियों आदि को समझना होता है। इसके लिए प्रयोज्यों (Interviewee) की अनुक्रियाओं को सावधानीपूर्वक साक्षात्कारकर्ता द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा साक्षात्कार के दौरान अशाब्दिक संकेतों को भी ध्यान में रखा जाता है। सामान्यतः सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु दो प्रकार के साक्षात्कारों का प्रयोग किया जाता है— संरचित साक्षात्कार (Structured Interview) तथा असंरचित साक्षात्कार ( Unstructured Inerview)
5.लम्बात्मक विधि (Longitudinal Method) इस विधि का प्रयोग ‘विकासात्मक मनोविज्ञान’ (Developmental Psychology) में किया जाता है। इस विधि में एक प्रतिदर्श को एक समय पर चुना जाता है तथा उनका अध्ययन लम्बे समय तक किया जाता है ताकि उस अंतराल में होने वाले विकासात्मक परिवर्तनों तथा विशेषताओं को समझा जा सके। उदाहरण के लिए एक शोधकर्ता 50 नवजात शिशुओं का अध्ययन करना शुरू करता है तथा लगातार 20 वर्षों तक उनका अध्ययन करता है (अर्थात् जब तक उनकी आयु 20 वर्ष हो जाए), तो इसे लम्बात्मक विधि का उपयोग कहा जाएगा। अतः लम्बात्मक विधि द्वारा किसी विशिष्ट अध्ययन को पूर्ण करने में ‘काफी लम्बा समय लगता है।
यद्यपि लम्बात्मक विधि में गुणात्मक रूप से महत्त्वपूर्ण परिणाम प्राप्त होते हैं इसकी मुख्य कमी यह है कि इसमें अत्यधिक समय खर्च होता है। इसके अलावा, प्रतिदर्श में से कुछ लोगों के दूसरी जगहों पर स्थानान्तरण के कारण तथा अन्य कई कारणों से प्रतिदर्श की हानि होती है।
शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र (Scope of Educational Psychology)
शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर 6 मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित है-
1.अधिगमकर्ता (Learner) शिक्षा मनोविज्ञान हमें अधिगमकर्ता को जानने की आवश्यकता से सामना कराता है साथ ही उसे बेहतर रूप से जानने के लिए तकनीकें उपलब्ध कराता है।
इसके अन्तर्गत निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित किया जा सकता है— व्यक्ति की जन्मजात क्षमताएँ, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ तथा उनका मापन, बाहरी, आंतरिक, चेतन व अचेतन व्यवहार (अधिगमकर्ता का), उसकी वृद्धि एवं विकास की विशेषताएँ- शैशवावस्था से लेकर वयस्कावस्था तक ।
2.अधिगम प्रक्रिया (Learning Process) अधिगमकर्ता को जानने के बाद तथा यह निर्णय लेने के बाद कि उसे किस प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करने हैं, अधिगमकर्ता द्वारा इन अधिगम अनुभवों को आसानी से तथा आत्मविश्वास से अर्जित कर पाने में सहायता करना एक सामान्य समस्या के रूप में उत्पन्न होती है। अतः इसके लिए अधिगम की प्रकृति को समझना तथा अधिगम प्रक्रिया किस प्रकार होती है यह जानना आवश्यक है। इसके अंतर्गत अधिगम के विभिन्न नियमों एवं सिद्धांतों के अलावा स्मृति तथा विस्मृति, प्रत्यक्षण, संप्रत्यय निर्माण, चिंतन, तर्कणा, समस्या समाधान, अधिगम का स्थानांतरण, प्रभावशील अधिगम के तरीके आदि के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है।
3.अधिगम परिस्थिति (Learning Situation)शिक्षा मनोविज्ञान उन वातावरणीय कारकों से भी सम्बन्धित होता है जो कि अधिगम परिस्थिति में सम्मिलित किये जाते हैं तथा अधिगमकर्ता एवं अध्यापक की अंतर्क्रिया पर प्रभाव डालते हैं। कक्षा का वातावरण, समूह-गतिशास्त्र तकनीकें तथा अधिगम को सुचारु बनाने वाले उपकरण, निर्देशन एवं परामर्श आदि बिन्दु जो कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की कार्यप्रणाली को आसान बनाने में सहायता करते हैं, अधिगम परिस्थितियों में शामिल किये जाते हैं।
4.शिक्षण परिस्थिति (Teaching Situation) शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षण की तकनीकों के भी सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं। इसके द्वारा यह निर्णय लेने में भी सहायता होती है कि अध्यापक द्वारा छात्रों की शारीरिक आयु व मानसिक स्तर के अनुसार किस प्रकार की परिस्थिति प्रस्तुत की जानी चाहिए। अधिगमकर्ताओं की विशेषताओं के आधार पर किस विषय में किस प्रकार की शिक्षण-अधिगम सहायक सामग्री उपयुक्त रहेगी, आदि ।
4.अधिगम निष्पादन का मूल्यांकन (Evaluation of Learning Performance) शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का चहुँमुखी विकास है। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष आते हैं । शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा आँकलन तथा मूल्यांकन हेतु विभिन्न उपकरणों तथा तकनीकों के सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं। इसका सम्बन्ध सिर्फ मापन से ही नहीं है, अपितुं परीक्षणों के क्रियान्वयन के बाद परिणामों का विश्लेषण करना, खराब निष्पादन के कारण पता लगाना,• कुसमायोजित बालकों को निर्देशन व परामर्श द्वारा सहायता प्रदान करना, परीक्षा तकनीकों, अधिगम शैलियों आदि का विश्लेषण करना तथा अधिगमकर्ता को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में सहायता देना भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है 1
5.अध्यापक (Teacher)शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के आवश्यक व्यक्तित्व गुणों, रुचियों, अभिवृत्तियों तथा प्रभावशील शिक्षण की विशेषताओं आदि पर भी बल देता है।
यह अध्यापक को अपने स्वयं के व्यक्तित्व को समझकर दबाव, द्वंद्व तथा दुश्चिंताओं का सामना करने में भी सहायता करता है।
Q.1-क्या मनोविज्ञान की किताबें हिंदी में भी होती हैं? Ans.-मनोविज्ञान क्या है , अर्थ :10 परिभाषायें New Tips and Tricks Psychology in hindi
दोस्तो हमारी टीम ने इस आर्टिकल में मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा,मनोविज्ञान का क्षेत्र,मनोविज्ञान की विधियाँ ओर मनोविज्ञान के सम्प्रदायको के बारे में विस्तृत जानकारी दी अगर आप हमारी दी हुई जानकारी से संतुष्ट है और आप इसी तरह की जानकारी रखना चाहते है तो आप हमारी वेबसाइट www.akstudyhub.com से जुड़े रहिये ओर अगर आप कोई सुझाव देना चाहते है तो हने कमेंट के माध्यम से दे सकते है ।
धन्यवाद…..







