जीवन (Life) क्या है ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मनुष्य सदियों से खोजता चला आ रहा है। जीवन वास्तव में एक विशेष स्थिति की अभिव्यक्ति है या एक प्रकार की शक्ति।
Characteristics Of Life – in Hindi
- Advertisement -
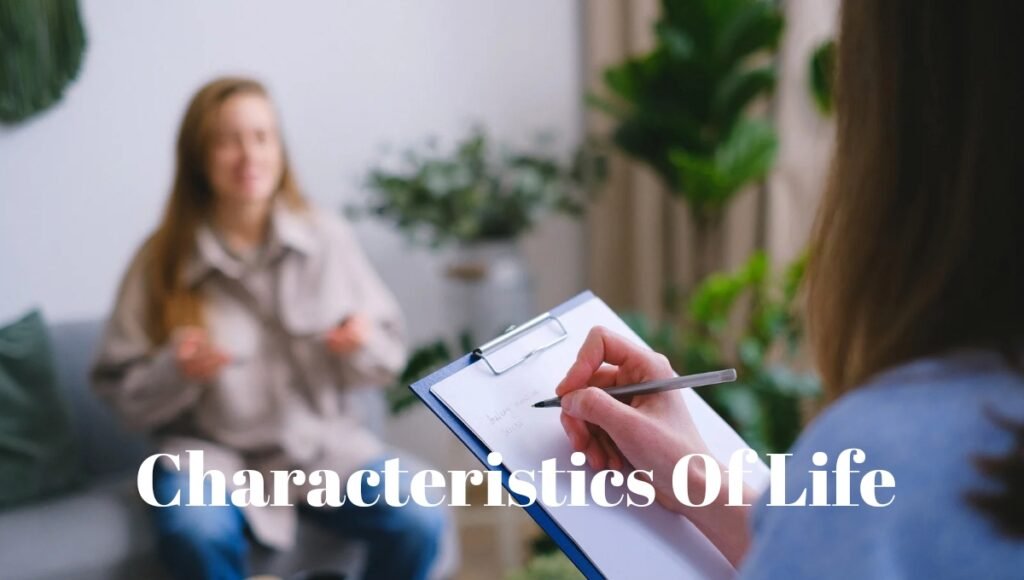
जीवन की कोई भी सीधी परिभाषा नहीं दी जा सकती है-हम इसका अनुभव कर सकते हैं किन्तु इसे न हम देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। जीवन अमूर्त (abstract) है किन्तु जीवन का होना या न होना हम सजीव तथा निर्जीव पदार्थों में भेद करके बता सकते हैं।
जीवन को एक शक्ति के रूप में माना जाता है जिसकी उपस्थिति में अथवा जिसके कारण जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं। तथा सजीव विभिन्न प्रकार के क्रिया-कलाप करते हैं। पृथ्वी पर पाये जाने वाले सभी पदार्थों को हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं।
Living & Non- Living

सजीव (Living Being) मनुष्य हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बन्दर, विभिन्न पेड़-पौधे जब तक जीवित रहते हैं, वे सजीव कहलाते हैं, क्योंकि इनमें वृद्धि, पोषण, श्वसन क्रिया, प्रजनन एवं निश्चित जीवन चक्र आदि जीवन के कुछ सामान्य लक्षण पाये जाते हैं।
निर्जीव (Non-Living) – मिट्टी, बालू, पत्थर, कोयला, रेलगाड़ी, मोटरगाड़ी, विभिन्न धातुएँ, विभिन्न पदार्थ; जैसे—तूतिया, फिटकरी आदि निर्जीव वस्तुएँ कहलाती हैं, क्योंकि इनमें जीवन के प्रमुख लक्षण, जैसे-पोषण, श्वसन, प्रजनन, निश्चित जीवन चक्र इत्यादि नहीं पाये जाते हैं। रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, जहाज आदि में गति के लिए बाहरी स्रोत से शक्ति प्राप्त होती है। तूतिया तथा फिटकरी के रवे में वृद्धि बाह्य कणों के जमने से होती
- Advertisement -
मृतक (Dead) – प्रत्येक जीवधारी की एक निश्चित जीवन अवधि होती है। जीवन अवधि के पूर्ण हो जाने पर उसकी मृत्यु मृत हो जाती है। मृत्यु के पश्चात् जीवधारी के शरीर को मृतक या शव कहते हैं। मनुष्य, पौधे एवं जन्तुओं के शरीर के अवशेषों का उपयोग करता है; जैसे—चमड़ा पशुओं की खाल से बनाया जाता है, लकड़ी पेड़ों के तने से प्राप्त होती है।
सजीवों के लक्षण (Characteristics of Livings)
Characteristics of livings सभी जीवधारियों में कुछ विशेष लक्षण पाये जाते हैं जिनके आधार पर उन्हें निर्जीव वस्तुओं से पृथक किया जा सकता है। ये लक्षण निम्नलिखित हैं
- निश्चित आकार तथा माप (Definite Shape and Size) – प्रत्येक जीवधारी चाहे वह जन्तु हो या पौधा उसका एक निश्चित आकार होता है। हाथी, शेर, घोड़ा, बन्दर, बिल्ली, कुत्ता, कौआ, कबूतर, केंचुआ, मक्खी, मच्छर आदि के नाम मात्र से उनको आकृति तथा माप का आभास हो जाता है।
इसी प्रकार आम, नीम, पीपल, खजूर, नारियल, सरसों, गेहूँ, चावल आदि के पौधों की एक निश्चित आकृति होती है। इसके विपरीत बहुधा निर्जीव वस्तुओं, जैसे—ताँबा, लोहा, पत्थर, सोना, चाँदी आदि का कोई निश्चित आकार नहीं होता है।
कुछ निर्जीव वस्तुओं जैसे -किताब, मेज, कुर्सी, पेण्ट, शर्ट, थाली, गिलास, रेलगाड़ी, जहाज,मोटरगाड़ी आदि को हम उनके आकार से पहचानते हैं। इन निर्जीव वस्तुओं को हम अपने उपयोग के लिए स्वयं एक रूप या आकार देते हैं।
- कोशिकीय संरचना (Cellular Structure) प्रत्येक सजीव (जन्तु एवं पौधे) एक या अधिक संरचनात्मक इकाइयों के बने होते हैं जिसे कोशा कहते हैं।
पौधों और जन्तुओं की सभी कोशाओं में जीवद्रव्य (protoplasm) कोशा कला (cell membrane) द्वारा घिरा रहता है। पौधों में इसके अतिरिक्त कोशा कला के बाहर एक निर्जीव कोशा भित्ति (cell wall) भी होती है। शरीर के विभिन्न भागों की कोशाओं के आकार भी भिन्न होते हैं,
परन्तु उनकी व्यवस्थित संरचना से प्रत्येक जीवधारी का शरीर बनता है। इसके विपरीत निर्जीव वस्तुओं में कोशिकीय संरचना नहीं पायी जाती है। निर्जीव वस्तुओं का निर्माण विभिन्न प्रकार के कणों से होता है।
Characteristics Of Life – in Hindi
- शारीरिक संगठन (Body Organization) सभी जीवधारियों का शारीरिक संगठन अनेक अंग (Organs) एवं अंग तन्त्रों (Organ systems) के द्वारा होता है।
इन्हीं अंग तन्त्रों के द्वारा विभिन्न जैविक क्रियाएँ; जैसे—श्वसन, पोषण, उत्सर्जन एवं प्रजनन आदि सम्पन्न होती हैं। निर्जीव वस्तुओं की संरचना उनके छोटे कणों अथवा भागों से होती है; जैसे—लोहा, सोना, चाँदी आदि की रचना उनके छोटे-छोटे कणों द्वारा होती है। मोटरकार, हवाई जहाज आदि को मनुष्य द्वारा निर्मित अनेक भागों को गठित करके बनाया जाता है।
- उपापचय (Metabolism) सभी जीवधारियों में हर समय बहुत-सी रासायनिक व भौतिक क्रियाएँ साथ-साथ होती रहती हैं। इन क्रियाओं में कुछ रचनात्मक (constructive) क्रियाएँ तथा कुछ विघटनकारी (destructive) क्रियाएँ होती हैं।
वे क्रियाएँ जिनसे शरीर के आवश्यक तत्त्वों; जैसे—जीवद्रव्य (Protoplasm), अस्थि, पत्ती, तने आदि का निर्माण होता है, उपचय (anabolism) क्रियाएँ कहलाती हैं। उपचय क्रियाएँ रचनात्मक होती हैं। इसके विपरीत अपचय (catabolism) क्रियाएँ विघटनात्मक या विनाशात्मक होती हैं ।
ग्लूकोज अथवा वसा के श्वसन द्वारा विघटन से ऊर्जा उत्पन्न होती है जो सभी जीव सम्बन्धी कार्यों के है संचालन के लिए आवश्यक है। उपचय एवं अपचय क्रियाओं का चक्र प्रत्येक जीवधारी में निरन्तर चलता रहता है। उपचय चक्र एवं अपचय चक्र को सम्मिलित रूप से उपापचय (Metabolism) कहते हैं ।
वास्तव में उपापचय ही जीवन का स्रोत है। इसी चक्र के द्वारा आहार ग्रहण करने की क्रिया पोषण, शरीर का निर्माण तथा अन्ततः श्वसन द्वारा ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। अतः कार्यिकी की दृष्टि से उपापचय ही जीवन के लक्षणों का सार है।
- श्वसन (Respiration) – प्रत्येक जीवधारी में श्वसन क्रिया हर समय होती रहती है। इस क्रिया में जीव वायुमण्डल से ऑक्सीजन (O) लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) बाहर निकालते हैं।
इस क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का ऑक्सीकरण (Oxidation) होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा से ही जीवधारियों की समस्त जैविक क्रियाएँ सम्पन्न होती हैं।
श्वसन क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है, किन्तु यह शरीर के सामान्य ताप पर होती है। इसमें कई जटिल एन्जाइमों की सहायता से अनेक रासायनिक प्रक्रियाएँ होती हैं। इस प्रकार के श्वसन को वायवीय श्वसन (Aerobic Respriation) कहते हैं। कुछ जीवों जैसे यीष्ट (Yeast) में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही श्वसन क्रिया होती है और ऊर्जा मुक्त होती है। इसको अवायवीय श्वसन (Anaerobic Respiration) कहते हैं।
- पोषण (Nutrition) – जीवद्रव्य के निर्माण के लिए और जीवधारियों की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीवधारी को जैविक क्रियाओं को सुचारु रूप से करने के लिए ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है।
पौधे पृथ्वी से जल, खनिज लवण और वायुमण्डल से कार्बन डाइ-ऑक्साइड लेकर हरित लवक की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जीव जगत में पौधे प्राथमिक उत्पादक (Primary Producers) कहलाते हैं। अन्य जीव-जन्तु अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं।
- वृद्धि (Growth) – किसी जीवधारी की आकृति, आयतन एवं शुष्क भार में बढ़ने को वृद्धि कहते हैं। पौधों में वृद्धि अनिश्चित समय तक विभज्योतिकी कोशिकाओं द्वारा निरन्तर होती रहती है और जन्तुओं में एक विशेष अवस्था आने पर रुक जाती है।
मनुष्य का शिशु धीरे-धीरे वृद्धि करके वयस्क बन जाता है, इसी प्रकार बीज के अंकुरित होने के पश्चात् नन्हा पौधा प्रौढ़ वृक्ष बनता है। वृद्धि के साथ ही जीव के अंगों का विकास होता है।
फिटकरी या नीले थोथे के रवे में वृद्धि अपर से इन्हीं पदार्थों के कणों के जमने के कारण होती है। निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि को बाह्य वृद्धि कहते हैं। जैसे-यदि तृतिये के संतृप्त पोल में पतले धागे से तूतिये का छोटा रवा (crystal) लटका दिया जाये तो वह दो-तीन दिनों में बढ़कर बड़ा हो जाता है।
- उत्सर्जन (Excretion) – जीवधारी के शरीर में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक ऐसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं; जैसे- अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइ ऑक्साइड इत्यादि। इन उत्सर्जन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन (Excretion) कहते हैं।
पौधों में भी अनेक उत्सर्जी पदार्थ: जैसे – गोंद, राल, टेनिन, कार्बन डाइ ऑक्साइड आदि बनते हैं। पौधे भी इन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते रहते हैं।
- गति (Movement) प्रायः जन्तु किसी न किसी तरह की गति करते रहते हैं। अंगों का हिलना-डुलना या जीवों का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना गति या गमन कहलाता है। जीवधारियों में यह गति भोजन की तलाश में अथवा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु होती है।
कुछ कोशिकीय पौधे जैसे—क्लेमाइडोमोनास (Chlamydomonas) एवं वॉलवॉक्स (Volvox) आदि पानी में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं, परन्तु अधिकांश पौधे एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, क्योंकि ये अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। सूर्यमुखी का पुष्प सूर्य की स्थिति के अनुसार अपनी स्थिति को बदलता रहता है।
निर्जीव वस्तुओं में गति बाह्य शक्ति के कारण सम्पन्न होती है: जैसे—-जहान, रेलगाड़ी में होने वाली यान्त्रिक गति बाहरी. ईंधन द्वारा उत्पन्न शक्ति द्वारा होती है।
- संवेदनशीलता तथा अनुकूलन (Sensitivity & Adaptability) – जीव जहाँ पर भी रहते हैं, अपने वातावरण में निरन्तर होने वाले परिवर्तनों को अनुभव करते हैं; (संवेदनशीलता) और उसके अनुसार अपनी संरचना एवं क्रियाओं में भी परिवर्तन करते हैं (अनुकूलन)। प्रत्येक जीवधारी में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने तथा इनके प्रति प्रतिक्रिया करने की शक्ति पायी जाती है।
Characteristics Of Life – in Hindi
यह प्रतिक्रिया जीवों की उत्तेजनशीलता के कारण सम्भव होती है; जैसे-गर्म चीज से अचानक हाथ छू जाने पर हाथ को तुरन्त हटा लेना। अधिक ठण्ड पड़ने पर चिड़िया अपने पंखों को खड़ा करके अपने शरीर को फुला लेती है। छुईमुई को पत्ती को छूते ही वह तुरन्त मुरझा जाती है। कोठभक्षी पौधे किसी कीट के सम्पर्क में आते ही उसे पकड़ लेते हैं।
- प्रजनन (Reproduction) प्रत्येक जीवधारी अपनी वंश परम्परा को कायम रखने के लिए अपने जैसी ही सन्तान उत्पन्न करते हैं, इस क्रिया को प्रजनन (Reproduction) कहते हैं। किसी भी जीव की सन्तान बहुत कुछ उसी के समान होती है ।
जैसे- आम के बीज से आम का ही पौधा पैदा होता है, कुत्ते के बच्चे से कुत्ते ही पैदा होते हैं।
- जीवन-चक्र (Life Cycle) प्रत्येक जीवधारी का एक निश्चित जीवन-चक्र होता है। जीवधारी के जन्म से मृत्यु तक घटनाओं का एक निश्चित क्रम होता है, उसे जीवन-चक्र (Life Cycle) कहते हैं। प्रत्येक जीवधारी का जीवन एककोशिका से प्रारम्भ होता है।
भ्रूणीय विकास के पश्चात् वह शिशु में परिवर्तित हो जाता है, जो वृद्धि के साथ-साथ किशोर, युवा, प्रौढ़ अवस्थाओं से गुजरता हुआ वृद्ध हो जाता है। अन्त में उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रत्येक जीवधारी की एक अनुमानित जीवन-अवधि होती है। निर्जीवों में इस प्रकार का कोई जीवन चक्र नहीं होता है।
जीव से जीव की उत्पत्ति (Life Highest Life)
सर्वप्रथम 1668 में फ्रांसिस्को रेड्डी (Franscisco Redi) ने बताया कि “जीव की उत्पत्ति जीव से ही सम्भव है।” उन्होंने अपने प्रयोग में कुछ मछलियों को उबालकर मृत किया। इन मृत मछलियों को छिन्न-भिन्न करके तीन जारों में छोड़ दिया।
एक जार को इन्होंने खुला छोड़ दिया तथा दूसरे जार को पार्चमेण्ट पेपर (Parchment Paper) तथा तीसरे जार को महीन जालीदार कपड़े से ढक दिया। कुछ दिनों बाद इन्होंने देखा कि पहले जार में माँस पर मक्खियों के लार्वा (Larvac) निकले तथा दूसरे और तीसरे जार पर लार्वा दिखायी नहीं दिये। प्रथम जार खुला होने के कारण माँस पर मक्खियों ने अण्डे दिये जिनसे लार्वा निकले। बन्द जारों में मक्खियाँ नहीं घुस पायीं।
Characteristics Of Life – in Hindi
इन पर लार्वा दिखायी नहीं दिये इस प्रयोग से इन्होंने सिद्ध किया कि मक्खियों के लार्वा सड़े-गले माँस में स्वतः उत्पादन से नहीं बनते बल्कि उन अण्डों से निकलते हैं जिन्हें मक्खियाँ माँस में रखती हैं।
इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही सम्भव है।
लुई पाश्चर (Louis Pasteur) ने 1862 में अपने प्रयोग द्वारा फ्रांसिस्को रेड्डी के मत का समर्थन किया। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक फ्लास्क लिया। उसमें यीस्ट और शक्कर के घोल को लेकर उबाला तथा फ्लास्क की गर्दन को गर्म करके “S” के आकार की खुली नहीं के रूप में मोड़ दिया।
इस फ्लास्क में भीतर जाने वाली हवा के सभी कण नली के मोड़ों पर ही चिपक कर रह गये और घोल में केवल शुद्ध वायु ही पहुँची। कुछ दिन इसी प्रकार फ्लास्क को रखा रहने पर भी इसमें कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हुआ।
इनके प्रयोग द्वारा यह पूरी तरह सिद्ध हो गया कि पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव-जन्तु स्वतः उत्पादन से नहीं बल्कि जल एवं हवा में पहले से उपस्थित जीवाणुओं और बीजाणुओं से बनते हैं।
उपरोक्त दोनों प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध होता है कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही सम्भव है।
यह भी पढ़े…
पारिस्थितिकी तंत्र |अर्थ,परिभाषा,घटक और खाद्य श्रंखला – Free Notes 2022-23
प्रजनन – जीव विज्ञान, प्रजनन के प्रकार |Reproduction – Free Notes 2022
https://www.vedantu.com/biology/living-and-non-living-thing
प्रिय पाठकों हमने अपने आर्टिकल Characteristics Of Life – in Hindi में सजीव ओर निर्जीव वस्तुओ के बारे में समझाया अगर आपको हमारा लेख अच्छा लगा तो आप हमारी वेवसाइट www.akstudyhub.com से जुड़े रहे
धन्यवाद….






