आज आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर देखें तो उसमें आपको हिंदी विषय के छन्द टॉपिक से कुछ न कुछ प्रश्न जरूर पूछें जाएंगे,
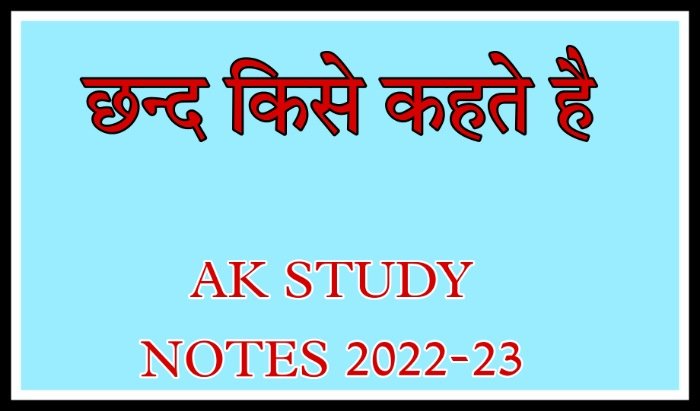
आज के लेख छन्द | छन्द किसे कहते है | छन्द की परिभाषा | छन्द कितने प्रकार के होते है – AK STUDY NOTES 2022-23 में आपको छन्द के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगें ।
- Advertisement -
छन्द का अर्थ और परिभाषा
‘छन्द’ शब्द की उत्पत्ति ‘छिदि’ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है- ढकना अथवा आच्छादित करना।
छन्द उस पद-रचना को कहते हैं, जिसमें अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा की गणना के साथ-साथ यति (विराम) एवं गति से सम्बद्ध नियमों का पालन किया गया हो।
छन्द के अंग
छन्दबद्ध काव्य को समझने अथवा रचने के लिए छन्द के निम्नलिखित अंगों का ज्ञान होना आवश्यक है
1.चरण
चरण या पाद छन्द की उस इकाई का नाम है, जिसमें अनेक छोटी-बड़ी ध्वनियों को सन्तुलित रूप से प्रदर्शित किया जाता है।
- Advertisement -
साधारणतः छन्द के चार चरण होते हैं—पहले तथा तीसरे चरण को ‘विषम’ तथा दूसरे और चौथे चरण को ‘सम’ चरण कहते हैं।
2. मात्रा और वर्ण
किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है, उसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। छन्दशास्त्र में दो से अधिक मात्राएँ किसी वर्ण की नहीं होतीं।
मात्राएँ स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं। यही कारण है कि मात्राएँ गिनते समय व्यंजनों पर ध्यान नहीं दिया जाता। वर्ण का अर्थ अक्षर से है, इसके दो भेद होते हैं ।
(क) ह्रस्व वर्ण (लघु) जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व वर्ण कहते हैं। छन्दशास्त्र में इन्हें लघु कहा जाता है। इनकी ‘एक’ मात्रा मानी गई है तथा इनका चिह्न ‘।’ है। अ, इ, उ तथा ऋ लघु वर्ण हैं।
(ख) दीर्घ वर्ण (गुरु)
जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्ण से दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ वर्ण कहते हैं। इन्हें गुरु भी कहा जाता है।
इनकी दो मात्राएँ होती हैं तथा इनका चिह्न ‘5’ है। आ, ई, ऊ, ओ, औ दीर्घ वर्ण हैं।
3. यति
छन्द पढ़ते समय उच्चारण की सुविधा के लिए तथा लय को ठीक रखने के लिए कहीं-कहीं विराम लेना पड़ता है। इसी विराम या ठहराव को यति कहते हैं।
4. गति
छन्द पढ़ने की लय को गति कहते हैं। हिन्दी में छन्दों में गति प्रायः अभ्यास और नाद के नियमों पर ही निर्भर है।
5.तुक
छन्द के चरणों के अन्त में समान वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं।
6. गण
| क्रम | गण | रूप | लक्षण | उदाहरण |
| 1 | मगण | sss | सर्व गुरु | नानाजी |
| 2 | यगण | lss | अति लघु बाद में दो गुरु | सवेरा |
| 3 | रगण | sls | आगे पीछे गुरु मध्य में लघु | केतकी |
| 4 | सगण | lls | प्रथम दो लघु अंत मे गुरु | रचना |
| 5 | तगण | ssl | प्रथम दो गुरु अंत मे लघु | आकार |
| 6 | जगण | lsl | आगे पीछे लघु मध्य में गुरु | नरेश |
| 7 | भगण | sll | प्रथम गुरु बाद में दो लघु | गायक |
| 8 | नगण | lll | सर्व लघु | कमल |
छन्द के भेद
मात्रिक छन्द और वर्णिक छन्द दो भेद है
मात्रिक छन्द
यह इन्द्र मात्रा की गणना पर आधारित होता है, इसलिए इसे मात्रिक छंद कहा जाता है। जिन छन्दों में मात्राओं की समानता के नियम का पालन किया जाता है।
किन्तु वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें मात्रिक छन्द कहा जाता है। दोहा रोला सोरठा, चौपाई, हरिगीतिका छप्पय आदि प्रमुख मात्रिक छन्द हैं।
1 चौपाई
परिभाषा चार चरण वाले इस सम मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में16 मात्राएँ होती हैं।
चरण के अन्त में जगण (ISI) अथवा तगण- (551) नहीं होता है। प्रथम तथा द्वितीय चरणों में ‘तुक’ समान होती है।
उदाहरण
बंदउँ गुरुपद पदुम परागा । सुरुचि सुवास सरस अनुराग
अमिय मूरिमय चूरन चारू । समन सकल भव रूज परिवारू
स्पष्टीकरण इस उदाहरण में चार चरण हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ तथा अन्त में दो गुरु वर्ण हैं। प्रत्येक चरण के अन्त में यति है। अतः यह चौपाई छन्द का उदाहरण है।
2.दोहा
परिभाषा दोहा अर्द्धसम मात्रिक छंद है।
इस छन्द के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। सम चरणों के अन्त में गुरु-लघु आते हैं।
उदाहरण
कागा काको धन हरै, कोयल काको देय।
मीठे बचन सुनाय कर, जग अपनो कर लेय।।
स्पष्टीकरण इस उदाहरण में चार चरण हैं। पहले (कागा काको धन हरे) और तीसरे (मीठे बचन सुनाय कर) चरण में 13-13 मात्राएँ तथा दूसरे (कोयल काको देय) एवं चौथे (जग अपनो कर लेय) चरणों में 11-11 मात्राएँ हैं। सम चरणों के अन्त के वर्ण गुरु और लघु हैं।
अतः यह दोहा छंद का उदाहरण है।
3. सोरठा
परिभाषा दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है।
यह एक अर्द्धसम परिभाषा छन्द है अर्थात् इसके पहले-तीसरे तथा दूसरे-चौथे चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है।
इसके विषम चरणों (पहले और तीसरे) में 11-11 और सम चरणों (दूसरे और चौथे) में 13-13 मात्राएँ होती हैं। तुक विषम चरणों में ही होता है तथा सम चरणों के अन्त में जगण (151) का निषेध होता है।
उदाहरण
“मूक होइ वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन।
जासु कृपा सु दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन।।”
स्पष्टीकरण इस उदाहरण के पहले चरण (मूक होई वाचाल) और तीसरे चरण (जासु कृपा सु दयाल) में 11-11 मात्राएँ हैं तथा दूसरे (पंगु चढ़े गिरिवर गहन) और चौथे चरण (द्रवौ सकल कलिमल दहन) में 13-13 मात्राएँ हैं।
विषम चरणों में तुक है तथा सम चरण के अन्त में जगण (151) नहीं है। अतः यह सोरठा छन्द का उदाहरण है।
4. रोला
परिभाषा यह एक सम मात्रिक छन्द है अर्थात् इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान रहती है।
चार चरणों वाले इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं तथा ग्यारह (11) और तेरह (13) मात्राओं पर यति होती है।
उदाहरण
कोउ पापिह पंचत्व, प्राप्त सुनि जमगन धावत ।
बनि बनि बावन वीर, बढ़त चौचंद मचावत।।
पै तकि ताकी लोथ, त्रिपथगा के तट लावत ।
नौ द्वै ग्यारह होत, तीन पाँचहि बिसरावत।।
स्पष्टीकरण इस उदाहरण में चार चरण हैं और प्रत्येक चरण में चौबीस (24) मात्राएँ हैं। ग्यारह (11) और तेरह (13) मात्राओं पर यति है। अतः यह रोला छन्द का उदाहरण है।
5. कुण्डलिया
परिभाषा यह विषम मात्रिक एवं संयुक्त छन्द है। इस छन्द का निर्माण दोहा और रोला के संयोग से होता है।
इसमें 6 चरण होते हैं। आरम्भ में दोहा और पश्चात् में दो छन्द रोला के होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं।
उदाहरण
कोई संगी उत नहीं है इत ही को संग।
पथी लेहु मिलि ताहि ते सबसों सहित उमंग।।
सबसों सहित उमंग बैठि तरनी कै माहीं।
नदिया नाव संजोग फेरि मिलिहै पहनाहीं ।
बरनै दीनदयाल पार पुनि भेंट न होई ।
अपनी-अपनी गैल पथी जो सब कोई।।
स्पष्टीकरण छ: चरणों वाले इस उदाहरण के प्रत्येक चरण में चौबीस (24) मात्राएँ हैं। इसका प्रथम चरण (कोई संगी) दोहे में प्रथम एवं द्वितीय चरण को मिलाकर रचा गया है
और इसके द्वितीय चरण (पथी लेहु ) की रचना दोहे में तृतीय व चतुर्थ चरण के सम्मिश्रण से हुई है। इसके अन्य चरणों की रचना रोला के चरणों को मिला कर की गई है।
इसमें यतियों की व्यवस्था दोहे एवं रोले के अनुसार ही है। अतः यह कुण्डलिया छन्द का उदाहरण है।
6. हरिगीतिका
परिभाषा इस सम मात्रिक छन्द के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएँ होती हैं तथा 16 और 12 मात्रा पर यति होती है। अन्त में लघु-गुरु का प्रयोग ही अधिक प्रचलित है।
उदाहरण
खग-वन्द सोता है अत: कल कल नहीं होता वहाँ।
बस मन्द मारूत का गमन की मौन है खोता जहाँ ।।
इस भाँति धीर से परस्पर कह सजगता की कथा।
यों दीखते हैं वृक्ष ये हों विश्व के प्रहरी यथा।।
स्पष्टीकरण यहाँ प्रत्येक चरण 28 मात्राओं वाला है, जिसमें 16 मात्रा पर यति है। अतः यह उदाहरण हरिगीतिका छन्द का है।
7.बरवै
परिभाषा इस अर्द्धसम मात्रिक छंद में कुल 38 मात्राओं वाले चार चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरणों में 12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 7 मात्राएँ होती हैं।
सम अर्थात् द्वितीय और चतुर्थ चरण में जगण (151) अथवा तगण (551) के प्रयोग से कविता सरल हो जाती है। यति प्रत्येक चरण के अन्त में होती है।
उदाहरण
तुलसी राम नाम सम, मीत न आना।
जो पहुँचाव रामपुर, तनु अवसान।।
स्पष्टीकरण यहाँ प्रथम एवं तृतीय चरण 12-12 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण 7-7 मात्राओं के हैं तथा सम चरणों के अन्त में जगण (151) है। अत: यह बरवै छंदका उदाहरण है।
वर्णिक छन्द
वर्णिक छन्दों की रचना का आधार वर्णों की गणना होती है। इसके तीन मुख्य भेद होते हैं- (i) सम (ii) अर्द्धसम (iii) विषम प्रमुख वर्णिक छन्दों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है
1. इन्द्रवज्रा
परिभाषा यह सम वर्णवृत्त अर्थात् सम वर्णिक छंद है। चार चरण वाले इस छंदके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण (अक्षर) होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण तथा 2 गुरु होते हैं। 11वें वर्ण पर यति होती है।
उदाहरण
तू ही बसा है मन में हमारे । = 11 वर्ण
तू ही रमा है इस विश्व में भी ।। = 11 वर्ण
तेरी छटा है मनमुग्धकारी । = 11 वर्ण
पापापहारी भवतापहारी ।। = 11 वर्ण
स्पष्टीकरण इस उदाहरण में 11-11 वर्णों वाले 4 चरण हैं तथा प्रत्येक = 11 auf चरण के 11वें वर्ण पर यति है। इसके प्रत्येक चरण में दो जगण, एक तगण एवं अन्त में दो गुरु हैं। अतः यह इन्द्रवज्रा छंद का उदाहरण
2. उपेन्द्रवज्रा
परिभाषा इस सम वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 2 जगण, 1 तगण तथा 2 गुरु होते हैं। 11वें वर्ण पर यति होती है।
उदाहरण
बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजै = 11 वर्ण
परन्तु पूर्वापर सोच लीजै ।= 11 वर्ण
बिना विचारे यदि काम होगा, = 11 वर्ण
कभी न अच्छा परिणाम होगा। = 11 वर्ण
स्पष्टीकरण इस पद्य के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और दो गुरु के कम से 11 वर्ण हैं; अतः यह ‘उपेन्द्रवज्रा छंद है।
3. मालिनी
परिभाषा यह सम वर्णवृत्त है। इसमें 15 वर्णों वाले प्रत्येक चरण में दो नगण, एक मगण तथा दो यगण क्रम से रहते हैं। यति 8 एवं 7 वर्णों पर होती है।
उदाहरण
प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है। = 15 वर्ण
दुःख-जलधि निमग्ना का सहारा कहाँ है। = 15 वर्ण
अब तक जिसको मैं, देख के जी सकी हूँ। = 15 वर्ण
वह हृदय हमारा, नेत्र तारा कहाँ है ।। = 15 वर्ण
स्पष्टीकरण यहाँ प्रत्येक चरण में दो नगण, एक मगण तथा दो यगण के क्रम 15 वर्ण हैं। अतः यह ‘मालिनी’ छन्द है।
4. वसन्ततिलका
परिभाषा यह सम वर्णिक छंद अर्थात् सम वर्णवृत्त है। इसके 14 वर्णों वाले प्रत्येक चरण में एक तगण (551), एक भगण (511), दो जगण (151) सहित अन्त में गुरु होते हैं। यति 8वें एवं 6वें वर्ण पर होती है।
उदाहरण
थे दीखते परम वृद्ध नितान्त रोगी, = 14 वर्ण
या थी नवागत वधू गृह में दिखाती । = 14 वर्ण
कोई न और इनको तज के कहीं था, = 14 वर्ण
सूने सभी सदन गोकुल के हुए थे ।। = 14 वर्ण
स्पष्टीकरण यहाँ 14 वर्णों वाले प्रत्येक चरण में क्रम से 1 तगण, 1 भगण, 2 जगण सहित 2 गुरु का विधान किया गया है। अतः यह वसन्ततिलका छन्द का उदाहरण है।
5. सवैया
परिभाषा इस सम वर्णवृत्त के प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण (अक्षर) होते हैं। सवैया छंद के कई भेद हैं; जैसे—मत्तगयन्द, सुन्दरी, सुमुखी, मनहर इत्यादि ।
उदाहरण
केशव ये मिथिलाधिप हैं जग जिन कीरति बेल बई है। = 23 वर्ण
दान कृपान बिधानन सों सिगरी वसुधा जिन हाथ लई है। = 23 वर्ण
अंग छः सातक आठक सों भव तीनहुँ लोक में सिद्धि भई है। = 23 वर्ण
बेदमयी अरु राजसिरी परिपूरनता सुभ जोग मई है।। | = 23 वर्ण
स्पष्टीकरण यहाँ प्रत्येक चरण में 23 वर्ण हैं तथा चरण का प्रारम्भ 7 भगण एवं अन्त 2 गुरु से हुआ है। अतः यह मत्तगयन्द छंद का उदाहरण है।
Samanya Hindi Notes PDF | सामान्य हिन्दी नोट्स पीडीफ – Free Download 2022
1000+ प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गयी रचनायें और हिंदी के प्रसिद्ध कवि [ Download PDF ] Easy Tricks






